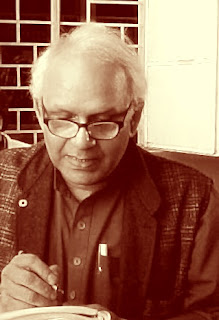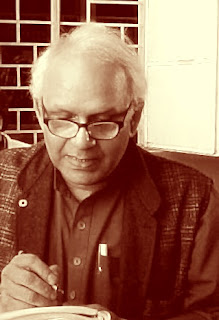राष्ट्रवाद की लूट है…
अजय तिवारी
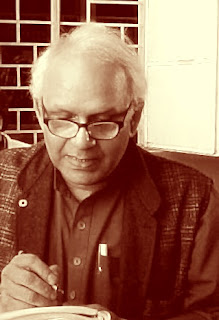 |
| अजय तिवारी |
राष्ट्र की सत्ता प्राचीन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा आधुनिक. राष्ट्र का अस्तित्व भूभाग-आबादी-भाषा-संस्कृति-इतिहास की साझेदारी पर निर्भर है, राष्ट्रवाद का इस विश्वास पर कि हम आपस में उद्देश्य, भावना या संस्कृति की साझेदारी रखते हैं. इसलिए राष्ट्र का जीवन विविधताओं के बीच एकसूत्रता से विकसित होता है, राष्ट्रवाद का विचार विविधताओं की अपेक्षा एकरूपता पर आधारित होता है. स्वभावतः राष्ट्र का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता लेकिन राष्ट्रवाद धर्म से जुड़ सकता है. ‘अहम् राष्ट्री संगमनी जनानाम’ से लेकर ‘भलि भारत भूमि भले कुल जन्म…’ तक जिस राष्ट्र का स्मरण है, वह कल्पना में नहीं, वास्तव में मौजूद है. ‘राष्ट्रवाद’ का विचार यूरोप से आया जहाँ उसका विकास पुनार्जगरण काल में मध्ययुगीन इसाई प्रभुत्व को चुनौती देने के साथ हुआ था. इसलिए धर्म से संवाद अथवा धर्म के स्वीकार-अस्वीकार का प्रश्न यूरोपीय राष्ट्रवाद की समस्या थी, भारत राष्ट्र की नहीं. आज जो लोग राष्ट्रवाद के विचार से धर्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे यूरोपीय साँचों को आरोपित कर रहे हैं.
यूरोप ने राष्ट्रवाद के उत्थान के दिनों में ईसाई महामंडल के विरुद्ध जातीय संस्कृतियों का परचम लहराया; ‘एक यूरोप’ की जगह फ़्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैण्ड, स्पेन आदि ‘राष्ट्रों’ (आधुनिक जातियों) का और उनकी भाषाओँ का आधार अपनाया. लेकिन साम्राज्य-विस्तार के साथ यूरोपीय राष्ट्रवाद अन्य जातियों और राष्ट्रों के उत्पीड़न का साधन बन गया. भारत ने अंग्रेजी शासन में राष्ट्रवाद के उत्पीडनकारी रूप का भरपूर अनुभव किया है. अंग्रेजों से लड़ते समय भारतीय देशप्रेमियों ने भी जिस विचारधारा का सहारा लिया, वह राष्ट्रवाद ही था. उत्पीड़नकारी देश का राष्ट्रवाद एक तरफ उत्पीड़ित समुदाय को विश्वास दिलाता है कि गुलामी उसके फायदे में है, दूसरी तरफ अपने समाज में उपनिवेशों की लूट से प्राप्त साधनों को राष्ट्रवाद के औचित्य के रूप में इस्तेमाल करता है. उसी तरह उत्पीड़ित समाज का राष्ट्रवाद विदेशी शत्रु को सामने रखकर एकजुट होने का प्रयास करता है. इस एकजुटता के लिए वर्तमान वंचना के अलावा अतीत के गौरव का सहारा भी लेता है. इसलिए उत्पीड़क राष्ट्रवाद में लक्ष्य और अवधारणा की एकरूपता मिलती है लेकिन उत्पीड़ित राष्ट्रवाद में अनेक धाराएँ और प्रवृत्तियाँ रहती हैं. उनमें सामंजस्य ही हो, यह आवश्यक नहीं है. खुद भारतीय राष्ट्रवाद में क्रन्तिकारी सुधारवाद से लेकर रूढ़िवादी पुनरुत्थानवाद तक अनेक अन्तर्धाराएँ विद्यमान रही हैं. बीसवीं सदी में आने के बाद भी एक तरफ नेहरु थे जो मानते थे कि राष्ट्रवाद ‘एक प्रति-अनुभूति’ है, वह ‘अन्य जातीय समुदायों के प्रति, विशेषतः सम्बंधित राष्ट्र के विदेशी हुक्मरानों प्रति घृणा या आवेश से’ जीवनी-शक्ति लेता है; दूसरी तरफ गोलवलकर थे जो कहते थे कि ‘हिन्दू-मुस्लिम एकता’ की बात करना ‘हमारे समाज के प्रति सबसे बड़े द्रोह का अपराध’ है, इसीलिए १८५७ के महासंग्राम में दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल बादशाह बहादुरशाह की ‘प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा’ को वे ‘अंग्रेजी राज से भी बहुत बड़ी दुखद घटना’ कहते थे.
इससे इतना तो प्रमाणित है कि राष्ट्रवाद के लिए एक वास्तविक या काल्पनिक, आतंरिक या बाह्य शत्रु अनिवार्य है जबकि राष्ट्र ऐसे शत्रु के बिना ही अधिक शांति और सौहार्द से विकसित होता है. नेहरु और गोलवलकर के परस्पर-विरोधी विचारों से यह साफ है कि स्वाधीनता आन्दोलन के समय से ही भारतीय ‘राष्ट्रवाद’ में अनेक अन्तार्धराएँ मौजूद रही हैं. विदेशी शासन के हट जाने के बाद राष्ट्रवाद का कोई वास्तविक आधार नहीं बचा. विकास के जिस रस्ते पर भारत चला, उसके संकट भूमंडलीकरण के दौरान अधिक तेज़ी से बढे. तब यह आवश्यक हुआ कि विषमतापूर्ण पूँजीवादी विकास को जारी रखने के लिए समाज में आतंरिक शत्रुओं का निर्माण किया जाय. इस बारे में सभी ‘राष्ट्रीय’ दल एकराय हैं. राजीव गाँधी की काँग्रेस ने शाहबानो मामले में मुस्लिम रूढ़िवाद को और रामजन्मभूमि मामले में हिन्दू रूढ़िवाद को प्रोत्साहन दिया. फिर क्या था, हिन्दू-मुस्लिम एकता को राष्ट्रद्रोह मानने वाली शक्तियाँ अचानक रंगमंच पर प्रभावशाली होने लगीं. आज की परिस्थितियाँ पिछले तीन दशक के इसी विकास का नतीजा हैं.
इस परिस्थिति की विडम्बना यह है कि मुस्लिम ‘राष्ट्रवादी’ यह नहीं देखते कि खुद पाकिस्तान का निर्माण भले ‘द्विराष्ट्र’ सिद्धांत से हुआ हो, जिसके जनक सावरकर थे और जिसका उपयोग जिन्ना ने किया, लेकिन पाकिस्तान का गठन इस्लाम के आधार पर नहीं हुआ था. उसे इस्लामी राष्ट्र बनाने का काम किया जिया-उल हक ने, जो अमरीका की मदद से सैन्य तख्ता-पलट द्वारा पदासीन हुए थे. लेकिन यह ‘इस्लामी’ राष्ट्रवाद अगर किसी के खिलाफ सिद्ध हुआ तो वह स्वयं पाकिस्तान है. इस्लाम के आधार पर वह बांग्लादेश को भी एक साथ नहीं रख सका, सिंध-बलोचिस्तान आदि को भी संतुष्ट नहीं रख पा रहा है. उसी तरह ‘हिन्दू’ राष्ट्रवादी यह नहीं देखते कि तमिलनाडु से असाम तक भारत की कोई आधुनिक संस्कृति नहीं है जिसमें अनेक धर्मावलम्बियों की मूल्यवान भूमिका न हो. खुद हिंदी में पहले कवि अमीर खुसरो हैं और पहले कहानीकार रेवरेंड जे. न्यूटन. तुलसी-मीराँ-प्रेमचंद-निराला का महत्व इन दोनों के बिना नहीं समझा जा सकता. इसलिए हमारी राष्ट्रीयता का वास्तविक स्वरुप हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवाद के काल्पनिक सिद्धांत से टकराता रहता है. विडम्बना यह है कि सत्ता में आने के बाद सांप्रदायिक राष्ट्रवाद विचारों की भिन्नता को ही राष्ट्रद्रोह बताकर दबाने लगता है. आज हम इसी बात का सामना कर रहे हैं.
यह मज़ेदार बात है कि धर्म से राष्ट्रवाद को जोड़ने का काम अमरीका, पाकिस्तान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तीनों ही करते हैं. जिस तरह भारत के ‘हिंदुत्व’ को उसके वास्तविक-उदार स्वरुप में विवेकानंद, मदनमोहन मालवीय और राधाकृष्णन ने समझा था, उसी तरह भारत की राष्ट्रीयता के धर्मेतर स्वरुप को गाँधी ने समझा था. उन्होंने उसे धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और जातीय (सांस्कृतिक) अंतर्वस्तु दी. यह अकारण नहीं है कि वे ‘सनातनी हिन्दू’ थे लेकिन उनकी हत्या एक ‘हिन्दुत्ववादी’ ने की! गाँधी का ‘हिन्दू’ भारतीय समाज का वास्तविक मनुष्य था, सावरकर का ‘हिन्दू’ एक काल्पनिक निर्माण. धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद इसी काल्पनिक निर्माण पर खड़ा होता है और उसे वास्तविकता पर आरोपित करता है. इसलिए वह उत्तेजना और अविवेक से परिचालित होता है. संकटकाल के क्षुब्ध मनोविज्ञान में इस ‘कल्पना’ को भी स्वीकार करने की सामाजिक प्रवृत्ति दिखाई देती है. कल्पना को वास्तविकता पर हावी करने के लिए मिथकीकरण का सहारा लिया जाता है. ज़ाहिर है, ऐसे में इतिहास को मिथक और मिथक को इतिहास में बदला जाता है. बैकुंठ को धरती पर अवस्थित करना या ऑपरेशन से गणेश के सर का प्रत्यर्पण मानना मिथक को इतिहास बनाने का उदहारण है, राणाप्रताप को विजयी दिखाना या पृथ्वीराज एवं शिवाजी को चक्रवर्ती मानना इतिहास को मिथक बनाने का. वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो तक्षशिला को ही उठाकर बिहार में स्थित कर दिया था! इस प्रक्रिया में इतिहास को अँधेरे में ठेलना अनिवार्य हो जाता है. बाबर के नामपर ‘राष्ट्रवादी’ राजनीति करते समय यह बात कब बताई जाती है कि बाबर भारत आना ही नहीं चाहता था, उसे अग्रहपूर्वक बुलाया था राणा साँगा ने, राजपूत सामंतों से त्रस्त होकर?
क्या यह पूछना अनुचित है कि दुनिया जब आपस में अधिक नजदीक हुई है, तब संकीर्णता और रूढ़िवाद पर आधारित राष्ट्रवाद क्यों आवश्यक है? क्या यह संयोग है कि कल तक अपनी पूँजी भेजने और प्रशिक्षित श्रम आमंत्रित करने के लिए ‘भूमंडलीकरण’ का दबाव डालने वाले देश आज खुद अपने समाज के संकट के चलते राष्ट्रवाद का आश्रय लेने लगे हैं? क्या यह स्मरण करना वाजिब है कि स्वाधीनता आन्दोलन के समय जो ‘भारतमाता ग्रामवासिनी’ थीं, वे कॉर्पोरेट पूँजी के समय ‘सेठसेविनी-दीनमर्दिनी’ हो गयी हैं तो इसका कोई आर्थिक पक्ष है? सास्कृतिक ‘राष्ट्रवाद’ की विडम्बना यह है कि जनता के आर्थिक प्रश्नों को पृष्ठभूमि में ठेलकर वह काल्पनिक उत्तेजना से समाज को भर देता है. तब ‘गोरक्षा’ से लेकर ‘मंदिर’ तक सभी कार्रवाइयाँ गिरोहों के हाथ में आ जाती हैं, सत्ता इन गिरोहों को राष्ट्रवाद के नामपर औचित्य प्रदान करते हुए जनता का दमन करती है और देशी-विदेशी कॉर्पोरेट की रक्षा में पलक-पाँवड़े बिछाती है. आज के राष्ट्रवादी विमर्श की यह सबसे प्रमुख विशेषता है.
****
संपर्कः बी-३०, श्रीराम अपार्टमेंट्स, ३२/४, द्वारका. नयी दिल्ली.११००७८
मो. ९७१७१७०६९३
हस्ताक्षर: Bimlesh/Anhad