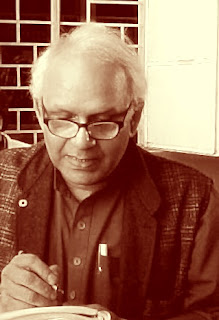युवा कवि रूपम मिश्र को 7 जनवरी 2023 को द्वितीय मनीषा त्रिपाठी स्मृति अनहद कोलकाता सम्मान प्रदान किया गया है। कवि को बहुत बधाई। ध्यातव्य कि सम्मान समारोह में युवा साथी मृत्युंजय जी ने रुपम की कविताओं पर चर्चा करते हुए जो बातें कहीं उसका आलेख रूप यहाँ प्रस्तुत है।
- संपादक मंडल

अँधेरे की डोर थामे उजाले की राह तलाशती कविताएँ :
मृत्युंजय पाण्डेय
रूपम मिश्र की कविताओं का जन्म ‘घृणा, खामोशी और दु:ख’ से हुआ है । कुछ घृणाओं को उन्होंने पैरों के तलवों से दबा रखा है और कुछ घृणाओं को अपने दोनों मजबूत हाथों से जकड़ रखा है । पैरों के तलवों के नीचे दबी हुई घृणा पितृसत्ता की धूर्तता है, जो वर्षों-वर्षों से चली आ रही है और हाथों से जकड़ी हुई घृणा स्त्रीवाद के नाम पर मर्दवादी समाज की नयी चालाकियाँ हैं । कमाल की बात यह है कि ‘घृणा की इस नयी धुन को स्त्री चीख-चीखकर गा रही है’ । उससे भी अद्भुत यह कि इस गान पर उस घृणा के जनक न सिर्फ तालियाँ पीट रहे हैं, बल्कि उसकी पीड़ित चिल्लाहट में अपना स्वर भी मिला रहे हैं । इन दोनों ‘घृणाओं का रंग इतना चितकबरा’ है कि कवयित्री समझ नहीं पाती—जो एक स्त्री भी है—कि ‘कौन-सा रंग झूठ का है, कौन-सा सच का’ । सफेद रंग के ऊपर न जाने कितने लाल-काले रंग पुते हुए हैं । पितृसत्ता और मर्दवादी समाज का स्त्री-विमर्श दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । चित भी उनका है पट भी उनका ।
रूपम मिश्र के यहाँ ‘खामोशी’ दो अर्थों में आई है । एक, जिन स्त्रियों की ये बात कर रही हैं वे भी खामोश हैं और उनकी खामोशी को देख अचरज से कवयित्री भी खामोश है । दरअसल यह खामोशी पितृसत्ता की देन है । शालीनता, मर्यादा और संस्कृति के नाम पर उनकी आवाज को हमेशा दबाकर रखा गया । ‘अधिकार’ के बदले उन्हें ‘कर्तव्य’ पढ़ाया गया । उनके लिए गांधी या नेहरू नहीं, बल्कि पिता और भाई ही दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं । गांधी या नेहरू के कथन से बढ़कर पिता या भाई का निर्देश है । इनकी पहचान पति के नाम से है । खुद की इनकी कोई पहचान नहीं । कवयित्री खुद से पूछती है—‘अपने अस्तित्व को लेकर इतनी उदासीनता क्या जन्मजात है यहाँ’ ? नाम की एक सामाजिक संरचना है—बचपन में फलाना की बेटी, विवाह के बाद फलाने की बीबी, माँ बनने के बाद फलाने की माँ, फलाने की बहू आदि-आदि । यह ‘फलाना’ उसके साथ आजीवन जोंक की तरह चिपका रहता है । स्त्री अपनी ही नजर में कुछ नहीं है । यदि कोई अपरिचित घर पर आ जाए तो वह कहती है घर में कोई नहीं है । स्त्री का अपनी ही निगाह में ‘कोई न होना’ दिल दहला देने वाली बात है । ‘हमारे नाम’ कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिये—
“मैं जो नाम के इतिहास को कुछ-कुछ जानती हूँ वह पासबुक लेकर मेरे पास आ गई हैं
बहुत संकोच से कह रही हैं दुलहिन इसमें मेरा नाम लिखा है क्या
मैंने कहा बताइये अम्मा आपका नाम क्या है
उन्होंने दो-तीन नाम लिए सोचते हुए कि
इसमें से ही कोई एक नाम मेरा है
बाकी मेरे बहनों के नाम हैं
वे इतनी सहजता से अपने नाम की पड़ताल कर रही थीं कि करुणा आवेग बनकर मेरे कंठ में रुक गई ।”
रूपम मिश्र ने अपनी कविताओं में पितृसत्ता और मर्दवादी समाज के इसी ‘कंकरही जमीन को दर्ज किया है—जिसके ऊपर वे खड़ी हैं—और जो उनके ‘पंजों में रह-रहकर चुभ’ रही है । उसकी चुभन इनसे बर्दाश्त नहीं होती । यह अच्छी तरह जानती हैं कि पुरुष अपनी सहूलियत के लिए ही मर्दवाद के नाश का बहकाऊ नारा लगा रहा है । वह पुरुषवादी समाज से कहती हैं यदि बात करनी ही है तो स्त्री जाति की नहीं उस सत्ता की करो ‘जिसने अपने गर्बिले और कटहे पैर से हमेशा मनुष्यता को कुचला है’ । लेकिन ये बात सत्ता की नहीं, स्त्री की करेंगे, जाति की करेंगे । स्त्री के लिए हदें तय करने वाले इस समाज से कवयित्री पूछती है, ‘होते कौन हो तुम, हमारी हदें तय करने वाले’ । एक कविता में वे कहती हैं—
“वे सभ्यता और समता की बात करते कितने झूठे लगते हैं
जो हमारी सौमुंहे साँप जो हमारी देह पर टेरीकॉट का ललका बुशर्ट भी देखकर
मुँह बिचकाकर कहते हैं; खूब उड़ रहे हो बच्चू, ज्यादा उड़ना अच्छा नहीं
उनसे कह दो कि अब तुम छोड़ दो यह तय करना
कि हमारा उड़ना अच्छा है या हमारा रेंगना
अब छोड़ दो टेरना सामंती ठसक का वह यशोगान
जिसमें स्त्रियाँ और शोषित की आह भरी है
मानव-जाति के आधे हिस्सेदार हम
जिनके आँचल में रहना तुमने कायरता का चिर प्रतीक कहा
अब दिशाहारा समय कुपथ पर है
संसार को विनाश से बचाए रखने के लिए
उनसे थोड़ी-सी करुणा उधार माँग लो ।”
रूपम मिश्र सीधे-सीधे, साफ लफ्जों में पितृसत्ता को चुनौती दे रही हैं । उस सत्ता को नकार रही हैं । वे कहती हैं जिसकी आँचल में छुपना तुम कायरता कहते हो उसी की करुणा से इस संसार को बचाया जा सकता है, तुम्हारी मर्दवादी सामंती सोच से नहीं ।
दु:ख के कई रंग हैं । कई रूप हैं । कुछ शौकिया दु:ख होते हैं तो कुछ प्रेम के । एक कवि के लिए प्रेम तो महत्त्व रखता है लेकिन उसका दु:ख नहीं । हो सकता है कुछ कवियों के लिए प्रेम का दु:ख ही जीवन का सबसे बड़ा दु:ख हो, लेकिन रूपम मिश्र अपने लिए प्रेम के दु:ख को नहीं चुनतीं । उनके पास दु:खों की एक लंबी सूची है किन्तु अपने लिए वे कुछ ही दु:खों का चुनाव करती हैं । कितनी चकित करने वाली बात है न दु:ख का चुनाव भी वे अपनी इच्छानुसार करती हैं । प्रेम के दु:ख से बड़ा उनके लिए उनके आसपास के ‘खुरदरे दु:ख’ अहमियत रखते हैं । कवि को उस माँ का दु:ख बड़ा लगता है जो अपने नवजात मृत शिशु को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती रही, जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करने के लिए डॉक्टर, नर्स और निर्जीव अस्पताल से गिड़गिड़ाती रही । इस खेत की बेटी के लिए ‘खेतिहरों के मटमैले दु:ख’ हर दु:ख से बड़े हैं । उसके लिए उन छोटी-बड़ी सहेलियों के दु:ख बड़े हैं, “जो जन्म लेते ही ब्याह के सपने’ देखने लगती हैं और एक दिन ‘हुक्मबाजों के नाम लिख दी जाती हैं’ । इस दु:ख की नदी में कवयित्री डूबने लगती हैं । उन्हें चारों ओर अँधेरा ही अँधेरा दिख रहा है, लेकिन उसी अँधेरे से वे उजाले की राह खोजती हैं और उस उजाले से धरती का एक कोना अंजोर कर देती हैं । वे खुद अँधेरे में खड़ी होकर ‘मुट्ठी भर-भए के अंजोरिया’ फेंकती हैं । कवयित्री के लिए धरती का एक कोना अंजोर करने से ज्यादा कठिन काम अँधेरे से लड़ना है क्योंकि उन्हें अँधेरे से बेहिसाब डर लगता है । वे कहती हैं—
लड़ाई की रात बहुत लंबी है
इतनी कि शायद सुबह खुशनुमा न हो
पर न लड़ना सदियों की शक्ल खराब करने की जवाबदेही होगी
हम असफल क़ौमें हैं
हमारी ही पीठ पर पैर रखकर वे वहाँ सफल हैं
जहाँ हमारे रोने को उन्होंने हास्य के बेहद सटीक मुहावरों में देखा
रूपम मिश्र के यहाँ ‘शालू सिंह’ और ‘वो लड़की’ दो ऐसी कविताएँ हैं, जो अलग राह दिखाती हैं । कवयित्री इन लड़कियों को उदाहरण की तरह पेश करती हैं । ‘शालू सिंह’ लड़की होकर स्कूल जाती है, वह बथुआ साग की तरह नहीं उगी थी, अपने घरवालों के लिए । वह गर्दन झुकाकर नहीं, साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाती थी । आँखों पर काला चश्मा, छोटे-छोटे बाल उन लड़कियों को खूब भाते थे, जिन्हें मर्यादा के नाम पर जकड़कर रखा गया था । ‘शालू सिंह’ को न जाने कितनी बार साइकिल से धक्का देकर गिराया गया, पर वह हार नहीं मानी । कवयित्री कहती हैं— ‘उस चलन की पुरनकी लड़ाई अब भी लड़ी जा रही है/ अब भी हमारे पूर्ण मनुष्य होने पर भी प्रश्नचिह्न रखे जाते हैं, शालू सिंह !’
‘शालू सिंह’ कविता का अगला कदम ‘वो लड़की’ है । इस कविता की लड़की गुड्डो-गुड्डियों से न खेलकर बिंदास गाँव की सड़कों पर बुलेट को दौड़ाती है और अपने ठोकर पर उन लड़कों को रखती है जिनकी माँ ने उन्हें मनुष्य बनना नहीं सिखाया । पहली बार साइकिल वही चलाती है, क्रांति की जमीन पर वही उतरती है । उसमें इतनी कुव्वत थी कि वह दुनिया को बदल सकती थी, लेकिन दुनिया ने उसे बदल दिया । उस ‘चकई’ की शादी एक बाज से कर दी गई । ‘साथ तो चकई और चकवे का होता है’ चकई और बाज का नहीं । कवयित्री कहती हैं
“मैंने गुजरात की नयी बनी दीवार नहीं देखी
पर जब वह देह के काले निशान को छुपाकर
झूठी हँसी हँसती है तो
मुझे लगता है कि मैंने देखी है
सच को ढकने वाली
नकली समृद्धि से पुती हुई वो चमकती दीवार !”
‘शालू सिंह’ कविता में पुरुष स्त्रियों के मनुष्य बनने पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है, लेकिन इस कविता में उसकी सारी मनुष्यता बे-फर्द हो जाती है । सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि विकास के भी खोखले वादों से आवरण हट जाता है । विकास किसका हुआ है ? सामंती सोचवाले पुरुषवादी समाज का तो हुआ नहीं ? वह आज भी वहीं है । उसे आज भी स्त्रियों के पर कतरने में आनंद आता है । उसे बोलती और उड़ती हुई स्त्री पसंद नहीं । वह उसे हर तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता है । बाज की उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई है । ये वही लोग हैं, जो प्रेम में पड़ी हुई लड़कियों को ‘फंसी हुई लड़कियाँ’ कहते हैं । इनके धूर्त प्रेमियों ने भी इन्हें फंसी हुई लड़की ही कहा । घर से भागी हुई लड़कियों को इन्होंने बेहाया कहा, लेकिन ये बेहाया नहीं थीं यदि ‘बेहाया होतीं तो फिर से इस समाज की छाती पर आकर उग जातीं/ वे तो बेहाया का हल्का नीला फूल थीं/ जिनके शीतल सौन्दर्य को देख धरती तृप्त होती है ।’
पितृसत्ता और सामंती सोच के साथ-साथ बाजार ने भी स्त्रियों का इस्तेमाल किया है । उन्हें मुक्त नहीं किया, बल्कि जकड़ा है । रूपम मिश्र की एक कविता है ‘पगहे’ । ‘पगहा’ पशुओं के गले में बाँधी जाने वाली उस रस्सी को कहते हैं जिससे उन्हें खूँटा पर बाँधा जाता है । पहले स्त्री के गले में पितृसत्ता के ‘जबर और दरेर’ पगहे थे । अब बाजार ने उस पितृसत्ता की रस्सी को चमकीला बना दिया है । कवयित्री कहती हैं—
हम इस नये पगहे को गले में लटकाये शान से घूमते
पुराने पगहे को कोसते
फिर जब ये पगहे कभी चुभते तो हम
फिर बाजार में ही हाजिरी लगाते
बाजार ब्रांडेड का हवाला देकर अपने और पास खींच लेता
रूपम मिश्र इस बात पर ज़ोर देती हैं कि ‘बाजार ने हम स्त्रियों को नये-नये दु:ख दिये’ हैं । बाजार ने उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया और वे नाचती रहीं और आजादी का गीत गाती रहीं । आज बाजार स्त्री को एक सामान बनाकर रख दिया है । न तो उसका अपने देह पर अधिकार है और न ही मस्तिष्क पर नियंत्रण । एक तरह से यह बाजार पितृसत्ता का ही बदला-आधुनिक रूप है । स्त्री के देह और मन पर उसका नियंत्रण आज भी बरकरार है । रूपम मिश्र इस चालाकी को समझ रही हैं । वे समझ रही है कि पूँजीवादी समाज में स्त्रियाँ दोहरी मार झेल रही हैं । पितृसत्ता से वे पूरी तरह अभी उबरी भी नहीं हैं कि बाजार ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है । उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उससे निकलने की कोई राह नहीं दिख रही । वे सभी स्त्रियों से पूछती हैं— ‘हम कब चीन्हेंगे अपने लिए बाजार में उतारी गई इनकी रंगीन डोरियों और पगाहों को’ ।
सवर्ण होते हुए भी रूपम मिश्र ने इस समाज की मानसिकता को खोलकर रख दिया है । उन्हें इस उद्धारक कुल में पैदा होने पर शर्म आती है । शर्म इस बात की है कि एक दलित को कुत्ते से भी ज्यादा ओछा समझा जाता है । घर में बर्तन में कुत्ता पानी पी लेता है, लेकिन अछूत के लिए अलग बर्तन की व्यवस्था है । उन्हें अपने मनुष्य होने पर तब ज्यादा शर्म आने लगती है जब वह ठठाकर हँसते हुए यह कहता है कि ‘हम लोग कुत्तों से बद्दतर जाति हैं’ । वह सवर्ण समाज से कहती हैं—
“शर्म आती है मुझे खुद के उद्धारक कुल में पैदा होने पर
संभ्रांत कुलीनता का बोझ ढोने पर
तुम नहीं सह पाओगे मेरी शर्म को
घृणा से पागल हो जाओगे
और अपनी गाली से सीखी भाषा को और पैनी करोगे ।”
शर्म उन्हें देश के ‘नंगे-उघरे लोगों’ को देखकर भी आती है । जिनके पास सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुँच पाती । योजनाएँ तो हजारों बनती हैं, लेकिन इनका ‘पेट इतना बड़ा है कि वह भरता ही नहीं’ । इधर हाल के कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने रात-दिन एक करके कई योजनाओं की शुरुआत की है । कवियात्री कहती हैं—
“और बेचारे राष्ट्र भाग्य विधाता को
अट्ठारह घण्टे काम का दावा करके भी
जनता से ही कहना पड़ा
कि आप ही करे इन भूखों-नंगों का इंतजाम
सरकार व्यस्त है लॉकडाऊन लागू करने में
और बेचारे प्रधानमंत्री ये तय करने में
कि अब अगला बॉलकानी कारनामा क्या कराऊँ !
ताकत कैसे दिखाऊँ ।”
 गांधी का आखिरी आदमी अब भी आखिर में ही खड़ा है । यदि सरकार चाहती तो उस आखिरी व्यक्ति से पंक्ति की शुरुआत कर उन्हें पहला बना सकती थी, लेकिन यहाँ तो गांधी की नहीं, बल्कि उन्हें मारने वाले की जयजयकार हो रही है । पर क्या यह वास्तविक जयजयकार है ? नहीं ! जयजयकार करने वाले भी जानते हैं कि सत्य क्या है ? गोडसे का नाम भले ही वे चीख-चीखकर लेते हों, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें जरूर धिक्कारती होगी । अभी भी सत्य सबसे ज्यादा चमकदार है और झूठ उसके पीछे दुबका हुआ है । यह कवयित्री का विश्वास है । वे कहती हैं— ‘अभी भी बच्चे चश्मा, लाठी और एक कमजोर सी देह की छाया देखकर उल्लास से कहते हैं—वो देखो गांधी !!’ गांधी के इस देश में न तो अहिंसा बहुत दिनों तक चल सकती है और न ही कारनामा ।
गांधी का आखिरी आदमी अब भी आखिर में ही खड़ा है । यदि सरकार चाहती तो उस आखिरी व्यक्ति से पंक्ति की शुरुआत कर उन्हें पहला बना सकती थी, लेकिन यहाँ तो गांधी की नहीं, बल्कि उन्हें मारने वाले की जयजयकार हो रही है । पर क्या यह वास्तविक जयजयकार है ? नहीं ! जयजयकार करने वाले भी जानते हैं कि सत्य क्या है ? गोडसे का नाम भले ही वे चीख-चीखकर लेते हों, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें जरूर धिक्कारती होगी । अभी भी सत्य सबसे ज्यादा चमकदार है और झूठ उसके पीछे दुबका हुआ है । यह कवयित्री का विश्वास है । वे कहती हैं— ‘अभी भी बच्चे चश्मा, लाठी और एक कमजोर सी देह की छाया देखकर उल्लास से कहते हैं—वो देखो गांधी !!’ गांधी के इस देश में न तो अहिंसा बहुत दिनों तक चल सकती है और न ही कारनामा ।
रूपम मिश्र ने प्रेम पर सर्वाधिक कविताएँ लिखी हैं । वह ये स्वीकार करती हैं कि प्रेमी के एक सम्बोधन पर उनका सारा स्त्रीवाद निसार हो जाता है । ऐसा अक्सर होता है, दो प्रेमियों के बीच विमर्श-बहस में प्रेम उनसे दूर “छिटककर एक कोने में सिसक रहा होता है’ । प्रेमिका सोचती है—‘उससे हाथ छुड़ाकर उठूँ/ और प्रेम को झाड-पोंछकर गोद में रख लू/ और निकल जाऊँ उसे बिना बताए कहीं !’ पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि आज भी प्रेमिकाएँ खुद को प्रेमी में ही ढूंढती हैं ।
प्रेमिका से पत्नी बनने के बाद भी एक स्त्री के लिए प्रेम में जिया गया हर पल खास होता है, उसे वह आजीवन सहेजकर रखना चाहती है । लेकिन इस खूबसूरत पल को उसका प्रेमी ही ‘पीड़ा, बेचैनी और दु:ख’ से भर देता है । ‘भीने संगीत से लरज़ रही रात को वह सिसकियों’ में बदल देता है । अंत में कहती हैं—‘प्रेम में प्राप्य कुछ भी नहीं’ । ‘तुम्हारा जाना’ कविता में कवयित्री कहती हैं—
“कुछ तमाशे तुम्हें और देखने थे !
सारी मोहरें तुम्हारे हाथ में थीं
चाहते तो खेल शुरू होने से पहले खत्म कर देते
पर कुछ तमाशे तुम्हें और देखने थे !!”
रूपम मिश्र अपनी कई प्रेम कविताओं में इस बात की ओर संकेत करती हैं कि प्रेमी-पुरुष के दो रूप हैं । दुनिया के सामने वह अपने असली रूप में नहीं बल्कि मुखौटा ओढ़े रहता है । वे प्रेमी ही होते हैं जो गिलहरी जैसी लड़कियों को, प्रेम के नाम पर बनारस, कोलकाता और नेपाल जैसी गलियों में बेच देते हैं । वे वर्षों-वर्षों से प्रेम में छली जा रही हैं, इसके बावजूद वे प्रेम करना नहीं छोड़तीं । वे पितृसत्ता के अँधेरे में खड़े होकर प्रेम रूपी उजाले की ओर हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन वह उजाला उन्हें अँधेरी गलियों में धकेल देता है । जहाँ उनकी चीख कोई नहीं सुन पाता । न तो वह घर की रहती हैं और न ही घाट की । पिता जीते-जी उनका श्राद्ध कर देते हैं । कवयित्री प्रेम के लिए एक ऐसे देश की कल्पना करती हैं—
जहाँ पारियाँ और तितलियाँ रहती हैं
जहाँ लोरियों में प्रेम के किस्से सुनाये जाते हो
जहाँ प्रेम के लिए भागकर जान न गवानी पड़ती हो
जहाँ एक विधवा और विकलांग को प्रेम हो जाने पर
सिर मुड़ाकर खालिक पोत गधे पर न घुमाया जाता हो
जहाँ प्रेमिका को मिलने उसके घर गया प्रेमी
जिंदा लाश बनकर न लौटता हो
जहाँ प्रेम हो जाना एक फूलों के उत्सव के रूप में मनाया जाता हो
जहाँ नदियां पाटी न जाती हों
हरे पेड़ काटे न जाते हों
जहाँ पिता कहता हो—ब्याह इतना भी जरूरी नहीं होता, मेरी लाड़ो !
जहाँ बुलबुले दु:ख की लोरी से सोती हैं और
डर, तिरस्कार की प्रभाती से जागती हैं
उनके रोने से धरती भीज रही है…!
रूपम मिश्र ने अपनी कविताओं में दूर की कौड़ी की खोज नहीं की है । उनकी कविताओं का संसार इतना जाना-पहचाना है कि मन विस्मित हो उठता है । भाषा में न तो कोई बाड़बोलापन है न चमत्कार । भाषा का कुछ नौमा देखिये— (1) मुँहजोरी भले घर की लड़कियों के लक्षण नहीं (2) मैं हमेशा टिकोरे के बीज को ऐसे चिटकाती (3) हम कब चीन्हेंगे अपने लिए बाजार में उतारी गई इनकी रंगीन डोरियों और पगाहों को (4) तुम बबुआने से पढ़ने आती थी, शालू सिंह (5) सारे शुकुलाने, तिऊराने, दुबाने, पड़ाने और तो और बबुवाने (6) सलीके से कटे बालों को वे लौंडाकट कह कर चिढ़ाते (7) उस चलन की पुरनकी लड़ाई अब भी लड़ी जा रही है (8) बिरहमिन ने कहा (9) खेतिहरों के मटमैले दु:ख (10) तुम यहाँ ज्यादा मालिकाना न दिखाओ (11) मुट्ठी भर-भर के अंजोरिया तुम्हारे ऊपर फेंकती (12) दर्द को दबाकर, एक भरभराई सी हँसी हँसती है (13) हमारा मालिक बहुत रिसिकट हैं (14) ये वही आखी-पाखी लड़कियाँ थीं, जिनके दु:ख धरती की तरह थे (15) और बज्र झूरे में बादल भी घुमड़कर नहीं बरसे कभी (16) हरजाई पतुरिया की बेटी है, बिना नाचे नहीं रहा जाता (17) गर्विले और कटहे पैर से हमेशा मनुष्यता को कुचला है (18) घुरहू चमार के डेहरईचा छूने पर सात पुश्तों को गाली देतीं (19) कल सबेरहिया रात में नींद खुल गई (20) बांसवारी वाले खेत में उग गईं रंग-बिरंगी मौसमी घास (21) गाय का चरा वन और बेटी का चरा घर फिर पनैपे तब जाना । रूपम मिश्र के यहाँ भाषा के ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएँगे । सबको यहाँ लिखना संभव नहीं है । रूपम मिश्र की भाषा सहज लोक-जीवन की भाष है । इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है ।
रूपम मिश्र की कविताओं का संसार ‘खगोल दुनिया के खुलते रहस्य की तरह न होकर’ ‘छुटपन में अचानक धूल में चमके अरुआ-परूआ पैसे की तरह’ है । आँखों में उसकी चमक आजीवन बरकरार रहती है । इनकी कविताएँ सहज-सामान्य स्त्री की कविताएँ हैं, जो अपना सारा जीवन चुपचाप बिता देती है । लेकिन इनकी कविताएँ सहज-सामान्य नहीं हैं और न ही वे चुप बैठती हैं । इन्होंने जिस जीवन को देखा है उसे ही कविताओं में उतार दिया है । यदि यह कहा जाए कि ये कविताएँ नहीं, बल्कि जीवन की पुनःव्याख्या है तो कुछ गलत न होगा । इनके पास स्त्री जीवन के अनगिनत किस्से हैं । उस अनगिनत किस्सों को इन्होंने बड़े ही जतन से संभालकर रखा है, जिसे वे धीरे-धीरे सुना रही हैं । लोककथा और बतकही के अंदाज में इन किस्सों को सुनाकर कवयित्री और सुनकर उनके पाठक दोनों उदास हो जाते हैं ।
***
मृत्युंजय पाण्डेय युवा आलोचक एवं अध्यापक हैं। वे कोलकाता में रहते हैं – उनसे pmrityunjayasha@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।